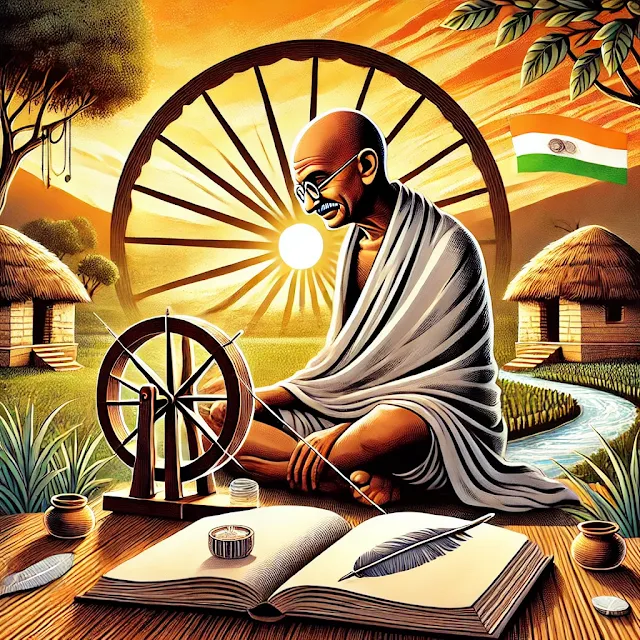आचार्य वासुदेवशरण अग्रवाल विभिन्न ज्ञानानुशासनों के सम्पुंजित विग्रह हैं। भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, इतिहास तथा भू-तत्व और लोक-विद्या का जितना गहन अनुशीलन आचार्य अग्रवाल ने किया था, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। उनका समूचा रचना-कर्म एक माहाकाव्य है जिसके प्रत्येक स्वर, वर्ण, शब्द, यति, अरोह-अवरोह, छंद और सर्ग में भारतीय मन और चिंतन के उदात्ततम स्वर प्रतिध्वनित होते हैं। भारतीय कला-दर्शन के संबंध में उन्होंने लिंग-मूर्ति या सर्वरूप प्रतिरूप चर्चा की है: “प्रतिरूप एक था रूप अनेक हैं, प्रतिरूप अमृत था. रूप मृत है, प्रतिरूप अपरिवर्तनशील था रूप परिवर्तनशील है। उस एक प्रतिरूप में सब रूपों का अंतर भाव है। गणित के शब्दों में यदि कहना चाहें तो सब अंकों की समष्टि शून्य है। अतएव यह भी चरितार्थ होता है कि जो सब रूपों को अपने में धारण करता है, वह स्वयं अणु है। जो मूलभूत प्रतिरूप है उसे निर्गत सूक्ष्म और स्थूल के नियम सभी काल में एक समान व्याप्त होते हैं। प्रतिरूप के अभिव्यक्ति प्रतीक द्वारा ही की जा सकती है। परंतु सर्वरूपमय प्रतिरूप के अभिव्यक्ति लिंग मूर्ति से ही हो सकती है। भारतीय शिल्पी किसी एक व्यक्ति विशेष का रूप नहीं बनाता, वह तो समाज में आदर्श के बिम्ब की कल्पना करता है।” स्वयँ उनका रचनात्मक व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही अनुपम और अपरिमित था, जिसकी छाया-प्रतिच्छाया में भारतीय ज्ञान-परम्परा की अनेकानेक स्थापनाएँ-मान्यतएँ और आदर्श प्रतिभाषित होती हैं।
(1)
आधुनिक हिंदी का जन्म और विकास भारतीय नवजागरण की कोख से हुआ। काव्य और कथा की कृतियों से पूर्व आधुनिक हिंदी वैचारिक और सामाजिक-सांस्कृतिक लेखन का माध्यम बन चुकी थी। ब्रजभाषा की सुकुमार कलाई जिन विचारों का भार वहन करने में लचक जाती थी, उसे आधुनिक हिंदी ने संभाल लिया। आधार भाषा के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खड़ी बोली के ताने-बाने पर रची यह भाषा बंगाल से पंजाब और हिमाचल से विदर्भ तक उत्तर-मध्य भारत के समूचे वितान पर मधुमालती की तरफ फैल गई। इसका बड़ा कारण उसकी यह क्षमता ही थी। उस समय के प्रत्येक व्यक्ति, समाज सुधारक, दार्शनिक, संस्कृति कर्मी की पहली चाहत थी एक ऐसी भाषा जो समूचे भारत को एक स्वर में संबोधित कर सके। जिसका स्वर भारत की चेतना को पुनर्गठित कर एकता दे सके। यह काम न तो तत्कालीन क्षेत्रीय भाषाएं, आंचलिक बोलियाँ और न पुरानी सरकारी जुबान फारसी या नई सरकारी गवर्निंग लैंग्वेज अंग्रेजी ही कर पा रही थी। इस अपेक्षा को पूरी करने के लिए हिंदी का वर्तमान मानक रूप अपेक्षा और दायित्व के छेनी और हथौडी से ही तराशा गया। मध्यकालीन संत कवियों के बाद भाषा को लेकर पहली बार इतनी छटपटाहट इस दौर में दिखाई देती है। कबीर और उनके समकालीन संत कवियों के समय में अरबी या फारसी इतनी सशक्त नहीं हुई थी, इसलिए भाषा को लेकर कबीर आदि कि बेचैनी का कारण मुख्यतः अभिव्यक्ति थी जबकि नवजागरण के दौर के बौद्धिकों के समकक्ष अंग्रेजी का सर्वग्रासी रूप मुँह बाए खडा था और उनकी भाषा सम्बंधी चिंता अपनी अस्मिता को बचाए रखने की चिंता थी। अपनी एक मुकरी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अँग्रेजी और अंग्रेजियत की ‘तारीफ’ इन शब्दों में की है:
सब गुरुजन को बुरो बतावै ।
अपनी खिचड़ी अलग पकावै ।
भीतर तत्व न झूठी तेजी ।
क्यों सखि सज्जन नहिं अँगरेजी ।
यह उस भारतीय मेधा के लिए सांस्कृतिक क्षरण के पूर्वाभास की तरह था, जिसकी परंपरा का आदर्श यह रहा हो :
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ।।
भारतेंदु ने जब यह लिखा कि ‘निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल’ तो उनका अभिप्राय भाषा-ज्ञान के साथ ही साथ भाषा में ज्ञान भी था । इसका प्रमाण उनकी रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका (पुरातत्त्व), कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय (इतिहास), संगीत सार और जातीय संगीत (संगीत), तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारत वर्ष (धर्म) आदि रचनाएँ हैं।
विदेशी भाषा के अधिपत्य के प्रभाव और उससे मुक्ति की चिंता तथा उसके यत्न भारतेंदु के बाद द्विवेदी युगीन लेखकों में भी देखी जा सकती है। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना और सरस्वती के प्रकाशन के साथ स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का चिंतन और लेखन के साथ ‘सरस्वती’ पत्रिका में परिलक्षित उनकी संपादन-दृश्टि इसकी साक्षी है। सरस्वती के जुलाई-अक्टूबर 1915 के अंक में प्रकाशित एक लेख ‘हमारे सामाजिक ह्रास के कुछ कारणों का विचार’ शीर्षक अपने लेख में माधव राव सप्रू ने अंग्रेजी शिक्षा और उसके प्रभाव पर कुछ इस तरह अपना विचार व्यक्त किया है, “विदेशी भाषा और विदेशी शिक्षा के आधिपत्य का परिणाम यह हुआ कि विदेशी हम लोग विदेशी भाषा में लिखते पढ़ते बोलते और विचार करते हैं। अंग्रेजी भाषा का सार्वत्रिक प्रचार ही हमारी भावी उन्नति के लिए आवश्यक समझा जाता है। हम अपने देश और समाज की दशा का विचार औरों की दृष्टि से किया करते हैं। फल यह हुआ कि पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा के रूप में हम लोग अपने आत्मभाव को कम कर डालने वाला और अपने समाज का ह्रास करने वाला काम करते चले जाते हैं और विशेषता यह है कि हम इसी को बुद्धि स्वातंत्र्य, सुधार, सभ्यता और उन्नति मान रहे हैं।...हम लोग विजतीय हो गए हैं।”
आजादी से पूर्व इस तरह की चेतना भारतीय समाज-सुधारकों, संस्कृति-चेतओं, लेखकों आदि में सहज लब्ध थी। दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, माधवराव सप्रे, चंद्र शर्मा ‘गुलेरी’, अध्यापक पूर्ण सिंह पद्म सिंह शर्मा, डॉ. मोती चंद, काशी प्रसाद जायसवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रभृत लेखकों के संपूर्ण लेखन का यदि एक साथ संग्रह कर उसका विश्लेषण किया जाए तो कोई संदेह नहीं रह जाता कि ‘निज भाषा’ या हिंदी को लेकर उसका उनका ‘विजन’ आज के हिंदी लेखन से कहीं ज्यादा व्यापक था। ऐसा करते हुए यह बार-बार दोहराए जाने की जरूरत होगी कि उनके लिए हिंदी ज्ञान, विचार और विमर्श की भाषा थी; केवल साहित्य भाषा नहीं। जिस निजता अथवा स्वत्व की गूँज यहाँ सुनाई पड़ती है, उसका संदर्भ अपनी भाषा के मार्ग पर खडे होकर ज्ञान-चक्षु खोलने से ही है।
आजाद भारत में सत्ता के रंगमंच पर अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजीयत धमक कमो बेस कायम रही । इसने हिंदी को ज्ञान का सहज माध्यम बनने से रोका। हिंदी लेखकों की अन्य ज्ञानानुशासनों के प्रति उदासीनता और सहित्येतर लेखन को हिंदी के विमर्श और आलोचना में कम मान देना भी एक बडा कारण रहा। फिर भी,आज हिंदी दुनिया भर में अपने प्रयोक्ताओं के बल पर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है तो उसके पीछे उन हिंदी सेवियों,, लेखकों और भाषा-साधकों का योगदान है, जिन्होंने साहित्य-मंडलों और हिंदी की अकादमिक दुनिया में अल्पचर्चित रहकर भी अपने जीवन का संपूर्ण स्नेह हिंदी की अखंड ज्योति के लिए समर्पित कर दिया।
(2)
इस परिदृश्य के बीच आचार्य वासुदेवशरण अग्रवाल की उपस्थिति विशेष महत्त्व रखती है। वे एक अनूठे ज्ञान साधक थे, जो एक सथ ही अनेक विद्याओं के मर्मज्ञ और अनेक भाषाओं में सम्भ्यस्त थे,। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों को अपने लेखन का माध्यम बनाया, किंतु उनके लिए किसी लेखक का गौरव उसके ‘पृथ्वी-पुत्र’ होने में है। इसलिए उनके लेखन का एक बडा हिस्सा हिंदी को समर्पित रहा। जायसी की कृति ‘पद्मावत’ के संजीवनी भाष्य में जायसी को ‘पृथ्वी पुत्र’ मानते हुए उन्होंने लिखा है : “जायसी सच्चे अर्थों में पृथ्वी-पुत्र थे। वे भारतीय जन-मानस के कितने सन्निकट थे, इसकी पूरी कल्पना करना कठिन है। गाँव में रहने वाली जनता का जो मानसिक धरातल है, उसके ज्ञान की जो उपकरण सामग्री है, उसके परिचय का जो क्षितिज है, उसी सीमा के भीतर हर्षित स्वर से कवि ने अपने गान का उँचा स्वर किया है। जनता की उक्तियाँ भावनाएँ और मान्यताएँ मानों स्वयँ छंद में बँधकर उनके काव्य में गुँथ गई हैं।” जनता की उक्तियाँ, मान्यताएँ और जीवन व्यवहार उसकी अपनी भाषा में ही होगी और जायसी ने उसी भाषा में उसे स्वर दिया है । आचार्य अग्रवाल जायसी के प्रति उनके मन में सम्मान और आत्मीयता है। वे जायसी की लोक-संसक्ति और लोक भाषा के प्रति लगाव के कायल हैं। अवध के जनपदीय जीवन से जायसी के लगाव और पद्मावत में उसकी सुन्दर अभिव्यक्ति के साथ ही अवधी भाषा और उसकी लोक वार्ताओं, लोकोक्तियों आदि के सटीक प्रयोग को आचार्य अग्रवाल ने सराहा है। वे इन्हें सहित्य का ज्योतिश्चक्षु मानते हैं। उन्होंने लिखा है “हिंदी भाषा के प्रबंध-काव्यों में जायसी का ‘पद्मावत’ शब्द और अर्थ दोनों दृष्टियों से अनूठा काव्य है । अवधी भाषा का जैसा ठेठ रूप और मार्मिक माधुर्य यहाँ मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है।” उनकी ये टिप्पणियाँ भाषा संबंधी उनकी मान्यतओं को व्यक्त करती हैं ।
गोस्वामी तुलसीदास अवधी साहित्य के दूसरे प्रतिमान हैं । कालक्रम की दृष्टि से जायसी के परवर्ती होते हुए भी साहित्यिक-सांस्कृतिक महत्त्व की दृष्टि से हिंदी समुदाय में उनसे अधिक लोकप्रिय और लोकप्रतिष्ठित हैं। अग्रवाल जी ने उनकी साहित्यिक-सांस्कृतिक भूमिका को रेखांकित करते हुए लिखा है: चतुर्भुज ब्रह्मा ज्ञान वेदी पर जिस प्रकार वेद चतुष्टयी का संगम होता है उसी प्रकार धर्म दर्शन साहित्य और पुराण रामचरित मानस में एक साथ मिले हैं । गोस्वामी जी ने जिस ज्ञान-यज्ञ का विधान किया, उसके मंडप में भारतीय वाङ्मय की समस्त परम्पराएँ अपने विशुद्ध और लोकहितकारी रूप में मिली हैं। इस मंडप के तोरण पर संगत और समन्वय का संदेश अंकित है ।... तुलसीदास की दूसरी बड़ी प्रतिज्ञा यह है कि नाना पुराण निगमागम सम्मत विशाल ज्ञान भंडार को तत्कालीन लोक भाषा में बद्ध कर के एक अति सुंदर निबंध के रूप में उसे जनता तक पहुंचाना है।” गोस्वामी जी को उनकी समन्वयशीलता, भक्ति और समजिक मर्यादा तथा लोकमंगल की प्रतिष्ठा की चर्चा हिंदी आलोचना में खूब हुई है। आचार्य अग्रवाल भी उनकी इस भूमिका को रेखांकित करते हैं, किंतु यह भी याद नहीं भूलते कि वे ‘लोक भाषा’ के कवि हैं। गोस्वामी जी जैसा संस्कृत भाषा का ज्ञाता और प्रयोग-निपुण कवि यदि देववाणी में ऐसी रचना करते तो निस्संदेह उत्कृष्ट होती और तत्कालीन विद्वत् समाज द्वारा प्रशंसित भी, लेकिन भारतीय साहित्य और संस्कृति में उनको वह प्रतिष्ठा नहीं मिलती जो एक लोकभाषा को आधार बनाकर वे पा सके : “भाषा छंद रस और अर्थ पर अपने असाधारण अधिकार का उपयोग यदि वह संस्कृत काव्य के लिए करते तो संभव यही है कि गोस्वामीजी उसमें भी सफल होते, किंतु उनकी उस सफलता से भी भारतीय साहित्य में एक बड़ा अभाव बना रह जाता जिंस भाषा को भदेस भृत्य कहकर विद्वान उस युग में हँसते रहे होंगे । उसमें यदि तुलसी ने अपने ‘अति मंजुल भाषा निबंध’ की रचना न की होती तो जनता और देश की प्राचीन संस्कृति के बीच में जो गहरी खाई बन गई थी वह पड़ी रह जाती है तुलसीदास का रामचरितमानस व सेतुबंध है जो जनता को और नाना पुराण निगमागम वाले साहित्य को आपस में मिलाता है।“
मध्यकाल के इन दोनों केंद्रीय कवियों की भूमिका को जिस परिप्रेक्ष्य में आचार्य अग्रवाल ने रेखांकित किया है, उसे देखते हुए भाषा के चुनाव और प्रयोग के प्रति उनकी सजगाता का पता चलता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता का आचर्य अग्रवाल का हिंदी भाषा में लेखन केवल संयोग या अनायास था। यह सायास और सजग लेखन है। जब आधुनिक ज्ञान के तमाम स्रोत अंग्रेजी भाषा में मौजूद थे और स्वयं अग्रवाल जी उस भाषा में अपने विचरों को व्यक्त करने में कुशल भी थे, तब उनके हिंदी प्रयोग का लक्ष्य हिंदी समाज की इतिहास, परंपरा और अधुनिक ज्ञान तक पहुँच सुनिश्चित करना ही था। इस दृष्टि से उनकी गणना भारतेंदु हरिश्चंद्र और महवीर प्रसद द्विवेदी के साथ करनी चाहिए। साहित्य, कला, इतिहास, पुरातत्त्व, सौंदर्यशास्त्र, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, लोक, शास्त्र जैसे विभिन्न ज्ञानुशासनों पर उनका लेखन हिंदी के ज्ञान-भंडार को जितना समृद्ध करता है, उतना हिंदी के किसी अन्य लेखक का नहीं, बल्कि उनका यह योगदान हिंदी की अनेक संस्थाओं से भी बडा है।
आचार्य वासुदेवशरण अग्रवाल भारतीय ऋषि-परम्परा के चिंतक थे। वे ज्ञान की अख़ंड सत्ता में विश्वास करते थे। उनकी अंतर्दृष्टि का विकास धर्म, दर्शन, अध्यात्म, व्याकरण कला, सौंदर्य, भूगोल, खगोल, लोक-विद्या आदि के गहन अनुशीलन से हुआ था। इसलिए भाषा और साहित्य की चर्चा करते हुए भी वे इन्हें साथ लेकर चलते थे। वे साहित्य की उपादेयता कला, मनोरंजन या आस्वाद-मात्र से अधिक मानते थे। भारतीय साहित्यकार विशेषतः हिंदी के साहित्यकार की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने लिखा है, “हिंदी लेखक को सबसे पहले भारत भूमि के भौतिक शरण में जाना चाहिए। राष्ट्र का भौतिक रूप आँख के सामने है। राष्ट्र की भूमि के साथ साक्षात्कार परिचय बढ़ाना आवश्यक है। एक-एक प्रदेश को ले कर वहाँ के पृथ्वी के भौतिक रूप का सांगोपांग अध्ययन हिंदी लेखकों को बढाना चाहिए। यह देश बहुत विशाल है।... देश की नदियां वृक्ष और वनस्पति, औषधि और पुष्प, फल और मूल, ऋण और लताएँ सब पृथ्वी पुत्र हैं। लेखक उनका सहोदर है।“ प्रकृति के प्रति उनका यह राग भारतीय लोक-मानस और आर्ष-चित्त का समन्वित उत्तरधिकार है। उन्होंने आगे लिखा है, “भारत के साहित्यकार विशेषतः हिंदी के साहित्य मनीषियों को चाहिए कि इस नवीन दृष्टिकोण को अपनाकर साहित्य के उज्ज्वल भविष्य का साक्षात दर्शन करें। दर्शन ही ऋषित्व है। ऋषियों साधना के बिना राष्ट्र या उसके साहित्य का जन्म नहीं होता।“ इन पंक्तियों को पढते हुए पाठक को ‘पृथ्वी सूक्त’ की अनुगूँज सुनाई पड सकती है, जो सहज है। आचार्य अग्रवाल पर इसका गहरा प्रभाव था। साहित्य और कला के प्रति उनकी दृष्टि तथा धरती के सौंदर्य के प्रति उनका अनुपम राग उत्तराधिकार में उन्हें यहीं से मिला था।
मातृभूमि के प्रति उनके अनुराग की बानगी , उनके मातृभूमि शीर्षक निबंध में देखी जा सकती है. “जिसके भाल पर कश्मीर-जन्मा कुसुम केसर तिलक है, जिसके पर जह्न तनया की एकावली है, जिनके चरणों में भक्तिभाव से अनवरत सिंहल प्रणाम करता है, जिसके चरणामृत का महोदधि नियमित पान करते हैं— उस माता के स्वरूप को जानने की किसे इच्छा न होगी? जिसके रक्षक स्वयं शैल राज हिमवंत हैं, जहाँ सरस्वती की शाश्वत धारा प्रवाहित है, जहाँ सिंधु और ब्रहृमपुत्र शैलराज के अमृत संदेश को अगाध सागर के समीप मंत्रणा के लिए ले जाते हैं, जहाँ मरुस्थल और दंडकारण्य जैसे विशिष्ट प्रदेश हैं— वह भूमि किस नाम से विश्रुत है?” यहाँ उनकी चित्रण शैली की विलक्षणता देखी जा सकती है, जो निर्विवाद रूप से साहित्यिक है। संस्कृत साहित्य की की इसपर गहरी छाप है और इसे हिंदी के ललित भंगिमा वाले निबंधों के साथ रखकर पढा जा सकता है। उनके अन्य निबंधों में भी भाषा अत्यंत सरस और सहित्यिक है। अपने गद्य में चित्र-भाषा का प्रयोग भी उन्होंने खूब किया है। इनमें उनकी रुचि और सहित्यनुराग भी परिलक्षित होते हैं।
राष्ट्रीयता और संस्कृति को साहित्य के अनुशीलन और मूल्यांकन को कसौटी मानना आचार्य अग्रवाल की साहित्य-दृष्टि की विशिष्टता कही जा सकती है। वे अपने सभी प्रिय रचनकारों को इस कसौटी पर जरूर कसते हैं। वाल्मीकि और तुलसीदास ही नहीं, वेदव्यास और कालिदास भी उनकी दृष्टि में यदि श्रेष्ठ कवि हैं तो अन्य तमाम विशिष्टताओं के साथ अपनी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भूमिका के कारण। महर्षि वेदव्यास के संबंध में उनकी मान्यता है कि “हमारे राष्ट्रीय अभ्युत्थान के लिए ‘महाभारत का विशेष महत्व है.... वेदव्यास जिस भारत राष्ट्र की उपासना करते थे, भविष्य का प्रत्येक हिंदू उसका स्वप्न देखेगा।” इसी तरह कालिदास के ‘रघुवंशम्’ महाकाव्य को उनका ‘राष्ट्रीय वैभव और आदर्शों का काव्य’ तथा उनकी कविता को ‘भारतीय संस्कृति की त्रिपथा गंगा’ कहना भी राष्ट्र और संस्कृति के प्रति उनके अनन्य राग का प्रमाण है। उनका राष्ट्र-बोध और सांस्कृतिक चेतना लोकानुरागी है। उनकी मान्यता थी कि “वही साहित्य लोक में चिर जीवन पा सकता है जिसकी जड़ें दूर तक पृथ्वी में गईं हैं। जो साहित्य लोक की भूमि के साथ नहीं जुड़ा, वह मुरझाकर सूख जाता है।” ‘महर्षि बाल्मीकि’, ‘महर्षि व्यास’, ‘महाकवि कालिदास’, ‘पाणिनि’, ‘तुलसी दास’, सूर दास, जायसी संबंधी उनका लेखन तथा ‘पाणिनिकालीन भारतवर्ष, ‘बाणभट्ट एक सांस्कृतिक अध्ययन’, हर्ष चरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन’, मेघदूत : एक अध्ययन, ‘भारत-सवित्री’, ‘कीर्तिलता : संजीवनी भाष्य’ ‘पद्वात: संजीवनी भाष्य’ उनकी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के साथ ही साहित्य-विवेक और ‘सहृदयता’ के साक्षी हैं।
अग्रवाल जी आधुनिक काल में भारतीयता के सम्भवतः पहले देशज सर्वांग भाष्यकार थे। पहले और देशज इसलिए कि वे भारतीयता के आत्म-तत्त्व के अन्वेषण में वेद-शास्त्रादि के अनुशीलन और अनुभावन के साथ ही लोक-मानस, लोक-धर्म, लोक-कला तथा लोक-जीवन को भी साथ-साथ लेकर चले और इन्हें ‘कल्प-वृक्ष’ की संज्ञा दी। उनसे पूर्व भारतीयता की आधुनिक समझ का एक बड़ा हिस्सा पाश्चत्य इतिहास दृष्टि और संकृति-बोध से प्रेरित या प्रभावित था। अध्येताओं ने वेद तथा धर्मशास्त्रीय ग्रंथों के मैक्समूलर आदि पश्चात्य विद्वानों द्वारा किये गए अनुवादों के आधार पर भारत की एक पाश्चात्य मूर्ति रची और फिर उसमें भारतीय संस्कृति की प्राण-प्रतिष्ठा के प्रयास किये। इसीलिए कुछ अध्येताओं को यह संस्कृति ‘आश्चर्यजनक’, ‘बेमेल’ या ‘अजायबघर’ सी जान पड़ती है। आचार्य अग्रवाल इनसे अलग इस अर्थ में हैं कि वे किसी पूर्वमान्यता के आधार पर साधारण प्रतिज्ञा के साथ नहीं चलते और न ही उसे सिद्ध करने की जिद करते हैं । उनका अध्ययन जन-जनपद-राष्ट्र के उत्तरोत्तर क्रम में आगे बढ़ता है और उनकी परस्पर अन्विति तथा अंतःसंबंधों की व्याख्या कर हमें भारतीय संस्कृति को पहचानने की आँख देता है।
आधुनिक शिक्षा द्वारा आरोपित औपनिवेशिक इतिहास दृष्टि जहाँ भारत की एक राष्ट्र के रूप में उपस्थिति के नकार और भारतीय संस्कृति के प्रति तिरस्कार की दृष्टि या दया की दृष्टि से देखने को प्रेरित कर रही थी, वहाँ आचार्य अग्रवाल उसके औदात्य को अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी समाज के सामने ला रहे थे। वे उपनिवेशवाद द्वारा अरो पित अंतरराष्ट्रीयता के समानांतर जनपदीय दृष्टि से भारत के अध्ययन की प्रस्तावना रच रहे थे। उनके ऐतिहसिक सांस्कृतिक अध्ययन की साधारण प्रतिज्ञा ही है कि “भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है।” और भारत ! आचार्य अग्रवाल के अनुसार, “भारत जनपदों का देश है।“ इसलिए भारत के राष्ट्र और संकृति के स्वरूप को उसके जनपदीय जीवन की समझ और उससे तादात्म्य के बिना नहीं समझा जा सकता। लेकिन दुर्भाग्यवश “पिछले दो सौ वर्षों में जनपदीय जीवन पर चारों ओर से लाचारी के बादल छा गए और उनके जीवन के सब स्रोत रुंध गए। अब फिर से जनपदों के उत्थान का युग आया है। देश के महान कंठ आज जनपदों की महिमा का गान करने के लिए खुले हैं। देश के राजनीतिक संघर्ष में ग्रामों और जनपदों को आत्मसम्मान आत्मप्रतिष्ठा और आत्म महिमा के भाव से भर दिया है।”
वासुदेव जी ने भारत की समझ के लिए जिस जनपदीय अध्ययन की आँख की चर्चा की है, उसकी ‘ज्योति भाषा है’। किसी भाषा-शास्त्री के लिए जनपदीय अध्ययन कल्प-वृक्ष या कामधेनु की तरह है। इसीलिए उन्होंने उक्त विषय पर लिखी गई अपनी पुस्तक का नामकरण भी ‘कल्प-वृक्ष’ ही किया है। इस दृष्टि से वे हिंदी और उसकी बोलियों के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते थे। हिंदी विकास और व्युत्पत्ति में ग्रियर्सन की तरह संस्कृत की भूमिका को सारा महत्व देने की तुलना में वे जनपदीय बोलियों की भूमिका को भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं, “हिंदी भाषा के शब्द निरुक्ति के लिए हमें जनपदीय बोलियों के कोषों का सर्वप्रथम निर्माण करना होगा बोलियों में शब्दों के उच्चारण और रूप जाने बिना शब्द की व्युत्पत्ति का पूरा पेटा नहीं भरा जा सकता। बोलियों की छानबीन होने के उपरान्त कई लाभ होने की संभावना है । प्रथम तो इन कोषों में हमारे प्रादेशिक जीवन का पूरा ब्योरा आ जाएगा, दूसरे शब्द नामक ज्योति जीवन के अंधेरे कोठों को प्रकाश से भर देगी और तीसरे जनपदों के बहुमुखी जीवन के शब्दों को पाकर हमारे साहित्यिक वर्णना शक्ति विस्तार को प्राप्त होगी। इन बोलियों की लोकोक्तियों के संग्रह पर उनका बल था । उनकी मान्यता थी कि ‘लोकोक्तियों के रूप में समस्त जाति की आत्मा एक बिंदु या कूट पर संचित होकर प्रकट हो जाती है।”
जिस समय आचार्य अग्रवाल हिंदी और उसकी बोलियों का अध्ययन समाज भाषा विज्ञान या तुलनात्मक भाषा विज्ञान की दृष्टि से करने की पहल कर रहे थे, तब हिंदी के अकादेमिक परिवेश में ये पद्धतियाँ सामान्य चलन में नहीं थीं। वे भारतीय शिक्षा पद्धति में इन लोकोक्तियों को शामिल करने के हिमायती थे, क्योंकि ये संस्कृति और भाषा की तरह ही लोक-जीवन के व्यवहार के लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं; “जनपदीय चक्षुष्मत्ता साहित्यिक का ही नहीं प्रत्येक मनुष्य का भूषण है उसकी वृद्धि जीवन की आवश्यकता के साथ जुडी है।”
आचार्य अग्रवाल मूलतः इतिहास और कला के अध्येता थे। उनके अनेक आलेख, शोध पत्र और ग्रंथ हिंदी भाषा में रचे गए। जबकि भारतीय भाषाओं में इस तरह के ज्ञान के प्राथमिक स्रोतों का अभाव था और हिंदी का सामान्य पाठक वर्ग उपनिवेशी इतिहासकारों की पुस्तकों का अनुवाद पढकर अपने देश और संस्कृति के बारे में राय तय करने लगा था, तब उनकी यह भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण थी। ऐतिहासिक और पुरात्त्विक साक्ष्यों के साथ साथ उन्होंने साहित्यिक ग्रंथों को भी अपने अनुसंधान का आधार बनाया, मार्कंडेय पुराण: एक सांस्कृतिक अध्ययन, पणिनि की ‘अष्टाध्यायी’ के आधार पर ‘पाणिनिकालीन भारतवर्ष’, बाणबट्ट की ‘कादम्बरी’ और ‘हर्ष चरित’ का सांस्कृतिक अध्ययन और महाभारत आधारित भारत-सावित्री इस तरह के अनूठे और अनुकरणीय उदाहरण हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने हिंदी के ज्ञान क्षितिज का विस्तार किया और ‘पृथ्वी सूक्त : एक अध्ययन’, ‘उरुज्योति’, ‘वेद्विद्या’, ‘वेदरश्मि’, ‘भारतीय कला’, पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, चक्रध्वज, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, कला और संस्कृति, भारत की मौलिक एकता, प्राचीन भारतीय लोकधर्म आदि नक्षत्रों के माध्यम से उसे प्रकाशित किया।
संदर्भ ग्रंथ :
1. अग्रवाल, वासुदेव शरण, कल्प-वृक्ष, साहित्य सदन, इलाहाबाद, 1952
2. अग्रवाल, वासुदेव शरण, भारत सावित्री, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, 1964
3. अग्रवाल, वासुदेव शरण, पाणिनिकालीन भारत वर्ष, चौखंभा विद्याभवन, वाराणसी,
4. अग्रवाल, वासुदेव शरण, हर्ष चरित: एक सांस्कृतिक अध्ययन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, 1953
5. अग्रवाल, वासुदेव शरण, भारतीय कला, पृथ्वी प्रकशन, वाराणसी, 1966
6. अग्रवाल, वासुदेव शरण, पृथ्वी-पुत्र, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, 1960
7. अग्रवाल, वासुदेव शरण, पद्मावत्, संजीवनी भाष्य, साहित्य सदन, चिरर्गाँव,झाँसी, 1956
8. त्रिपाठी, आचार्य राममूर्ति, वासुदेव शरण अग्रवाल, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली, 2009
9. पांडेय, मैनेजर (सं.), माधवराव सप्रे :संकलित निबंध, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2009
10. वात्स्यायन, कपिला (सं), वासुदेव शरण अग्रवाल रचना संचयन, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली, 2012
11. शुक्ल, हनुमानप्रसाद (सं.), राष्ट्र धर्म और संस्कृति, प्रभात प्रकशन, नई दिल्ली-2023
- विश्व हिन्दी पत्रिका, मारिशस 2024 में प्रकाशित